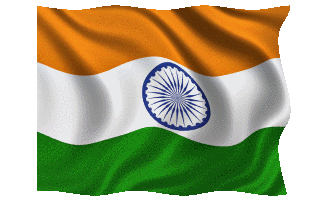अग्निशेखर हिंदी के क्लासिक कवि हमारी धरोहर

सुशील कुमार अग्निशेखर हिंदी के क्लासिक कवि हमारी धरोहर
अग्निशेखर आधुनिक हिंदी के क्लासिक कवि हैं। उनकी कविताओं में विस्थापन के भोगे हुए सत्य का जो विस्तार दिखता है, वह हृदय को मथकर रख देती है। मानवीय संवेदना का इतना गहन प्रसार हमें केवल निराला और रवीन्द्रनाथ टैगोर की रचनाओं में मिलता है। यहाँ जीवन-सत्य जितना मर्मभेदी है, उतना ही पीडा आपूरित ।
"मैंने भूखडों को जलते देखा है"
उबलते हुए समन्दरों में मैंने देखा है
नदियों का चीखते-कराहते हुए उतर डूबना
गिरना जहरीले पानियों के गाजों का
किंतु रहा फिर भी मैं जिन्दा
मैं पैदा हुआ हूँ जिन्दा रहने के लिए ही
(तिलचट्टा किसी भी समय )
"इच्छाएं मेरा घर थीं"
तमाम उम्र रहा अकेला उनमें
संसार की तमाम कब्रों में
दफन हूं मै
आकांक्षाओं के साथ
सपनों की मिट्टी है मेरे ऊपर
(तमाम उम्र कालवृक्ष की छाया में)
'खगाल रहे हैं आंसूओं को
गोताखोर
आपदा के तल में बहुत मोती हैं
इस समुद्र पर सब की आँख है।
(भूकंप के बाद भुज कालवृक्ष की छाया में)
जब हम ऐसे समय में जी रहे हों, जहाँ सच्ची कविताएँ नकली कविताओं से विस्थापित और बेदखल हो रही हो तो ऐसे समय में किसी प्रामाणिक और सच्चे कवि का बेदखल हो जाना कोई बड़ी बात नहीं।
मैं कवि अग्निशेखर के बरअक्स अपनी बात रख क्या यह सही नहीं कि कविता में विस्थापन रहा और पलायन की भावसत्ता कई बार कवि के महज शौक से उत्पन्न होती है? कितने कवियों ने अपनी छूटती हुई जमीन के बारे में भोगे हुए सत्य का दर्शन अपनी कविता में कराया है? किन आलोचकों ने जलावतनी पीड़ा के काव्य-सौंदर्य को अपनी कलम दी है ? अग्निशेखर की कविताओं से गुजरते हुए मैं महसूस करता हूँ कि इनमें विस्थापन उनके जीवन का वह भुक्त यथार्थ है, जिसमें न सिर्फ समय की बेतरतीब टीस मौजूद है, जो हमें कारुणिकता से आप्लावित कर देती है, बल्कि उनकी काव्यात्मकता भी हमें उतनी ही मोहती और बेचौन करती है। यह लोकजीवन के उस संघर्ष की व्यथा-कथा है, जो द्वंद्व के उस छोर पर लाकर हमें खड़ी करती है, जहां हम मानवीय मूल्यों की शिनाख्त के लिए बेचौन हो उठते हैं। नीचे इमेज फाइल में इनकी एक कविता देखिए
मुझसे छीन ली गई मेरी नदी
मुझसे छीन ली गई मेरी नदी
मुझसे छीन ली गई मेरी नदी
बदल दिया गया उसका नाम
बंद हो गया उसमें दियों का बहना
मुझसे छीन ली गई चिनार की छाह
उसका कर दिया गया लिंग परिवर्तन
वह थी मेरी भुवन व्यापिनी माँ
उसके रोम रोम से मुस्कुराती थी
मेरे सपनों की कोंपलें
एक दिन चुपचाप बदल दिए गए
मेरे सैकड़ों गाँवों के नाम
जैसे आँख मूदकर पहुँचा दिया गया हो
किसी अरब देश में
मुझसे छीन ली गई मेरी भाषा
छीलकर फेंक दी गई उसकी लिपि
इस तरह सदियों की ठंड में
बर्फ होती कभी गयी मेरी आवाज
मुझसे छीन लिया गया मेरा चेहरा
और सब तरफ से
पहचान लिये जाने के डर से
मैंने बदल लिया हुलिया
और घूमता रहा गलत फहमी में बेखौफ
मुझसे छीन ली गई धीरे धीरे
बर्फ, पहाडिया, मुस्कान
पेड़, मौसम, त्योहार
और समूची मातृभूमि अबकी बार
इस कविता की तरह ही इनकी बहुत सारी कविताएँ हैं, जो कवि के विस्थापन का जिया हुआ यथार्थ है, जो हमें कागजी कविताओं से न केवल अलग करता है, बल्कि उस भावजगत से हमारा साक्षात्कार भी कराता है जहाँ विस्थापन का गहराता हुआ मर्मभेदी लोकस्वर दूर से निकट आती और बरजती हुई क्रमशः तेज होती, कुरेदती हुई, हिलाती हुई, झिझोरती हुई बेकस ध्वनियाँ हैं।
अग्निशेखर की कविताओं से गुजरते हुए हमें मानव-विस्थापन के जिस रूप और रीति का साक्षात्कार होता है, वह केवल मर्मी ही नहीं, मर्माहत भी करता है। वह प्रभावोत्पादकता में जितनी वीभत्स रूप का वरण करती है, उतना ही करुणामय और हृदयविदारक भी महसूस होती है। गोया कि विस्थापन के कई रूप होते हैं। एक रूप होता है विकास की बाढ़ में लीलती संस्कृति का। पर इससे उजडते गाव-घर वनवासी, लोग-बाग की व्यथा-कथा इत्यादि उतनी विद्रूप और टीस भरी नहीं होती, जितनी सत्ता प्रभुओं के नियोजित जनसहार (जीनोसाइड) के फलस्वरूप जान बचाकर शरणार्थी शिविरों में भागकर आए गुजर-बसर करते, जैसे-तैसे अपने दिन काटते, अपनी दुःख-दैन्यता और संस्कृति की दुर्दशा से कराहते और जिल्ल भोगते समाज की । इस विस्थापन में सत्ता प्रभुओं द्वारा केवल जीव-सहार ही नहीं किया जाता, बल्कि साथ-साथ उसका एक पूरा कल्चरल जीनोसाइड भी कर दिया जाता है। यह कोई विकासवादी सांस्कृतिक प्रत्यावर्तन नहीं, बल्कि उसके सम्पूर्ण विरासत का अपहरण और उसकी निर्मम हत्या है, जिसका सामाजिक विस्तार केवल उसके डेमोग्राफिक स्तर तक नहीं जाता, बल्कि वह उसके इकोलॉजिकल और भौगौलिक लेयर को भी छूता है। वह वहाँ की प्रकृति में भी उसी तरह ध्वनित होता है।
अग्निशेखर ने अपने पहले काव्य संग्रह किसी भी समय (1992) में ही कश्मीर के निर्वासन और जीनोसाइड का संकेत दे दिया था। देखने वाली बात यह है कि इस संग्रह की सभी कविताएँ उनके विस्थापन के पूर्व की हैं। पर आगत समय को भाँपकर कवि का इन्द्रियबोध इतना प्रखर और चेतस हो गया लगता है। कि उसे कविता में आने वाले समय की आहट पहले ही मिल जाती है, जबकि कश्मीर में आने वाले सैलानी अभी तक भावी आतंक, हिंसा, विस्थापन, विखंडन, स्मृति विलोपन और मध्यकालीन बर्बरता के पुनरागमन के पूर्वाभास से बेखबर थे। तभी तो शेखर कहते हैं
कि -
दया करो सैलानियों के सौंदर्यबोध पर
फिल्मी कवियों के दारिर्थ पर
वे पानी के नीचे कैद आइसबर्ग के
सतह पर आते शब्दों को
बुलबुले कह रहे हैं।
झील ने छिपा रखी है इतनी बड़ी बात
(कविता जादुई झील पृ. 37 )
पुनर्वास और विस्थापन के कई आन्दोलन और उसके कवियों से जुड़े इस देश में कोई सबसे दुख-कातर बात हो सकती है तो वह यह होगी कि -
एक सम्पूर्ण लूटी-पिटी विस्थापित जाति के घाव
बसना चाहते हैं तुम्हारे संवेदन के घर में
कहीं उन्हें जबकि जलावतनी में यहाँ
नहीं मिल रहा एक चिथडा तबुं भी
बिना लस्त पस्त होने के
वे तलाशते हुए कहाँ-कहाँ फिरेंगे
खानाबदोशों की तरह
सास लेने की जगह
मेरे भारत महान में
कहाँ सुरक्षित रहेंगी इस धूप और पानी में
सैकड़ों गठरियों में बंधी
अभिनवगुप्त और कल्हण की पांडुलिपिया
ललद्यद और नादिम की कविताएँ
इस महाविपदा में तुम नहीं रहे हमारे साथ
जैसे तुम थे ही नहीं यहाँ इन दिनों
(कविता अपने ही सरोकारों से पृ. 36 )
सच में यह कवियों के लिए कितनी बड़ी चुनौती है कि एक सम्वेदना का मकान आज के हिंदी के अधिकाश कवियों के यहाँ भी जुदा हो गया है। कवि अपनी एक लघु कविता में व्यक्त करता है कि
'बंद हैं खिड़कियां सहस्रमुखी कविताओं की
चुप हैं शब्द अपनी-अपनी सीपियों में
हमारी लहूलुहान दस्तकें नहीं हैं मानवेतर
कि घबराकर दूर भागते हो। तुम
(कविता: इस महाविपदा में पृष्ठ 35)
किन्तु अग्निशेखर के कवि ने इस जोखिम को • स्वीकार ही नहीं किया, बल्कि वहां के लोगों के विस्थापन को अपनी कविता में आवाज दी और पहली बार चुप्पी की पम्परा को तोड़ने की पहल की। यह हिंदी साहित्य में अजूबा और अकेला ही है। किसी कवि के लिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। अब तक उनके पाँच काव्य संग्रह विस्थापन और अलगाववादी प्रवृत्तियों की अन्तरवस्तुओं पर आ चुके हैं। इनका दूसरा संग्रह मुझसे छीन ली गई मेरी नदी (1996), तीसरा 'कालवृक्ष की छाया (2002), चौथा जवाहर टनल' (2008) और पाँचवाँ जलता हुआ पुल' (2019) हैं। प्रसंगवश कहना चाहूंगा कि अग्निशेखर ने अपनी कविता 'जवाहर टनल' पर चयनित जम्मू कश्मीर कला. संस्कृति और भाषा अकादमी का सर्वश्रेष्ठ पुस्तक का अवार्ड यह कहते हुए लेने से ठुकरा दिया कि कश्मीरी जन सड़क पर हैं, हम कैसे अवार्ड लें, जिसके तहत 51 हजार रुपये का नकद पुरस्कार, स्मृति चिन्ह और शाल भेंट किया जाता है।
खैर, यहां इनकी कविताओं पर बात आगे बढ़ाते हुए कहना चाहता हूँ कि विस्थापन के दर्द को अभिव्यक्त करने के लिए वे कविता में जिन प्रतीकों, बिम्बों और कहन के शिल्प को समेटते हैं, वह हिन्दी में विस्थापन की कविताओं में विरल प्रतीत होता है। उनमें जितना बौद्धिकता का बल है, उतना ही भावों का उद्रेक। यहाँ लोक के शब्द इतने जीवत हैं कि वह हमारी आत्मा को मथकर रख देते हैं। वस्तुतः ये विस्थापित पीड़ित जनों के जीवनधर्मी बिम्ब हैं, जो उनके जीवन संघर्षो और द्वन्द्वों से जन्मते हैं। इसलिए उनकी पीड़ा में हमें एक आत्मिक खिंचाव की अनुभूति होती है जो आजकल के शहराती कवियों में शायद नहीं मिलेगी।
"झेलम मुझे पाकिस्तानी जासूस की तरह लगती है"
और मैं नींद में महसूसता रहा कि जमीन खिसक रही है।
ये पंक्तियों इस बात को बताती हैं कि एक नदी के पाकिस्तानी होने और कवि की नींद में उसके जमीन के खिसकने का अभिप्राय क्या है। एक कविता चिनार देखिए कवि कश्मीर की गोद में खेलता हुआ .अनंद-प्रमोद नहीं मनाता। वह वितस्ता नदी के रुपहले. पहलुओं में नहीं जाता, बल्कि चिनार से कई सवाल करता है। यह कविता जितनी संकेतात्मक है, उतनी ही मर्मभेदी
चिनार! तुम्हें कैसा लगता है
बहती थी जो तुम्हारे सामने से होकर
चादनी की चादर सी
मैली हो गई है अब वितस्ता
वितस्ता में अब नहीं बहते झिलमिलाते दिए
पूजा के फूल
जगह-जगह सूने पड़े हैं स्नान घाट
किसी विधवा की जैसे रूसीयाई माग
मैंने बहुत दिनों से तुम्हें भी
नाभी तक पानी में उतरकर सूरज को
जल चढ़ाते नहीं देखा है
तुम कहा धोते हो कपड़े लत्ते
हाथ-मुह
क्या पीते हो
चिनार ।
असह्य है तुम्हारे लाखों
बातुनी पत्तों की खामोशी (कविता चिनार -1)
अग्निशेखर बहुत कलात्मक ऊचाई से कविता में लोकसिक्त मुहावरों को रखते हैं, जो उनके अपने शब्द की निर्मिति हैं और उनमें कला के साथ भाव का अपूर्व संयोजन है, जिसके फ्यूजन से कविता पाठक प कबीराने अंदाज में बिना तल्ख हुए अपना गहरा छाप छोड़ती है।
ठगी हुई मछयारिन दृष्टि, विधवा की माग, ठिठुरती चेतना की तमाम सीढ़ियाँ, हिजड़ों की तरह बेशर्म नाचती हुई गिरती बर्फ, लोहे का चेहरा चढ़ाए मिहिरकुल, कीलों में जड़े जूतों मे गोरे गाँव, चील के पंजों में पकड़े साँप, नींद के जंगलों को टापों तले रौंदता घोड़ा आदि अनगिनत ऐसे मुहावरे और बिम्ब इस पहले ही संग्रह की कविताओं में आई हैं, जो हिन्दी कविता में अन्यत्र दुर्लभ हैं। ये कविताएँ पाठक के मन में विस्थापित हो गए लोक का एक ऐसा भावलोक रचती हैं जो भय, आतक त्रासदी झेल रहे जन के जीवन और संस्कृति को बचाने की मुसलसल जद्दोजहद व तडप से पैदा होती है। यहां जीवन स्थिर और मौन नहीं, रागात्मक और गतिशील है जो अपने अस्तित्व के संघर्ष की निर्मिति का नाम है, जिनकी नींव पर ये कविताएँ कम अज कम खड़ी हैं।
अग्निशेखर की कविताओं में प्रकृति के बिम्ब विस्थापन की भावभूमि पर आकर जो रूप लेते हैं, वह दुःख, भय, त्रासदी और आशा के बीच के अतद्वंद्व को जिस काव्यात्मक सौष्ठव और मेधा के साथ प्रकट करते हैं, वह पाठक के मन में कई भावों-अनुभावों का एक मिश्रित हिलोर या कम्पन (मिक्स्ड वाइब्रेशन) पैदा करता है, जैसे कि
छलनी छलनी मेरे आकाश के उपर से
बह रही है
स्मृतियों की नदी ओ मातृभूमि !
क्या इस समय हो रही है।
मेरे गांव में वर्षा? कविता वर्षा
यहाँ आकाश का बिम्ब कवि-पात्र की जमीन से अलगाव की पीड़ा के लिए व्यक्त हुआ है और नदी उसकी स्मृति के लिए। आकाश यानी स्वतंत्रता के छलनी- छलनी होने का दुःख सीधे अपनी जमीन और संस्कृति से छूटने का दुःख है। आप यह भी देखते हैं कि कविता में जमीन से नदी का न बहकर आकाश के ऊपर से बहना जिस प्रकृत्यात्मक विलोम में अर्थ-स्फीतियाँ उत्पन्न करती है, उसकी व्याप्ति कवि के उस अवचेतन मन अर्थात उसकी स्मृति में है, जिसमें वह अपने छूटे हुए गांव में वर्षा की आशा करता है और इसके मानिंद अपनी मातृभूमि से सवाल भी करता है। इस तरह यहां एक ही बिम्ब से जातीय प्रेम (ethnic attachment) के साथ विस्थापन की पीड़ा को सामने लाने का जो दुहरा काव्य - उपक्रम किया गया है, वह काव्य-बिम्बों के शिल्पगत प्रयोग की उत्कृष्ट बानगी है।
जीवन के रागात्मक द्वंद्वों और दुद्धर्ष संघर्षो को व्यक्त करने वाला कवि कभी प्रकृति का सुकुमार' कवि नहीं बन सकता। उसके यहाँ प्रकृति उसके जीवन के साथ इस तरह से अंतर्ग्रथित होती है कि प्रकृति के काव्य-उपकरण कवि-जीवन के अनुभवों से एकाकार हो उठते हैं।
महसूस होता है कि कविता की अंतर्वस्तु ब बाह्यगतता से आत्मगतता की ओर प्रसारित होती है। इसके उलट, जिस कवि का लोकानुभव कमजोर होता है, उसकी अंतर्वस्तु चेतना से निकल कर बाहर की प्रवाहित होती है, जिससे इन्द्रिय-चेतस मन बाह्य उपकरणों से तादात्म्य स्थापित नहीं कर पाता । फलतः रचना अपनी स्वाभाविक छटा खोकर आत्मबद्ध हो जाती है। इससे रचना में ऊब और तनाव का सृजन होता है, संघर्ष और श्रम का नहीं। यह बुर्जुआ सोच से रची गई कविताओं में अधिक पाया जाता है
उक्त परिप्रेक्ष्य में आप पाएंगे कि जिस प्रकार सु भीर सक्सेना की कविताओं में प्रकृति स्त्री-प्रेम का उपकरण बनकर आती है, जैसे शम्भु बादल की कविताओं में वह प्राकृतिक उपादानोंय पशु-पछियों से जनविद्रोह के प्रस्फुटीकरण का रूप लेकर आती है, अग्निशेखर भी उसी प्रकार प्रकृतिगत बिम्बों से विस्थापन व आतंक के सौंदर्य (एस्थेटिक्स ऑफ टेरर) को कविता में अभिव्यजित करने का काम लेते हैं।
गरजते बादलों
और काँधती बिजलियों के बीच
स्तब्ध है
मेरी अल्पसंख्यक आत्मा
वहीं कहीं अधजले मकान के मलबे पर
जहाँ इतने निर्वासित बरसों की उगी घास में
छिपाकर रखी जाती हैं
पाकिस्तान से आई बंदूकें
यहाँ किसे बख्शा गया मेरे देश में
निर्दोष होने के जुर्म में
तैरती हैं आज भी हवा में
दहाडे मारती स्त्रियों की बददुआएँ'
आज के दिन कोई आए मेरे पास
ले जाए मुझे
किसी पहाड़ी यात्रा पर
मैं छूना चाहता हूँ
एक नया और ताजा आकाश
( कविता काला दिवस)
यहाँ निर्वासित बरसों की उगी घास में बंदूकों का छिपा रहना उसी बाह्यगत अनुभव का हिस्सा है। कह सकते हैं कि शेखर जी अपनी कविता में मंगलेश डबराल जी की तरह कोई पोएटिक एक्रोबैटिक्स पैदा नहीं करते, बल्कि कवि के उसी पोएटिक स्किल से ही वह गुण प्रकट हो पाता है जिसकी ऊपर चर्चा की गई है। पर यह सब कवियों के वश की बात नहीं होती। गोया कि आजकल कवि तुरत-फुरत आत्मश्लाघा हो जाते हैं, यही कारण है कि अनुभवहीन आत्मबद्ध कविताएँ अब थोक में लिखी जा रही हैं।
यही नहीं, अग्निशेखर की कविताओं की अंतर्वस्तु वस्तुत उनके उस स्वभुक्त यथार्थ का हिस्सा है जिसमें जलावतनी पलायन की मार्मिक अभिव्यक्ति कश्मीर के परिवेश के सामाजिक तल के उस कोण से परिलक्षित हुई है, जहा आलोचकों ने अब तक एक रूटीन तौर पर ही काम किया है। उनमें ध्वनित लोकबिम्बों और विरल ख्यालातों पर लोगों की नजर कम ही गई है। खासियत यह है कि सघन जीवनानुभव और इन्द्रिय-बोध 1 से निःसृत इन कविताओं में विस्थापन के जो रागात्मकताएं हैं, वे रूप और कथ्य दोनों स्तरों पर दुःख की हमें भर्तृहरि के गीत की तरह आलोड़ती हैं। इसमें केवल वर्तमान के क्षण का ही स्पदन नहीं महसूस होता, हुतात्माओं की स्मृतियों और शहीदों का अनुभव भी दृष्टिगत होता है, जो अग्निशेखर के कवि को इस अर्थ में महत्वपूर्ण बनाता है कि वह लोक-विस्थापन के सबसे अलग और विशिष्ट कोटि का सौंदर्य रचते हैं। यह उनके समकालीनों में कहीं मिलता भी है तो इतनी काव्यात्मक गतिकी के साथ नहीं, आप स्वयं कवि का जीवन- इनकी एक कविता देखिए कविता लिखना
तपे हुए लोहे के घोडे पर चढना है
या उबलते हुए दरिया में
छलाँग मार कर मिल आना
उन बेचैन हुतात्माओं से
जो करते हैं
हमारी स्मृति में वास
पूछना उनसे शहीद होने के अनुभव
और करना महसूस अपने रक्त में
उनके नीले होठों पर दम तोड़ चुंके
शब्दों को
यह कविता मेरे समय में
किस कागज पर उतारी जा सकती है
अपने खुलते हुए लहू से
सिवाय बलिवेदी के
ऐसे कवि का जीवन
आकाँक्षा मेरी...
(कविता रू कवि का जीवन)
शहीदों के नीले होठों पर दम तोड़ चुके शब्दों को कागज पर उतारना इस कविता में एक नवीन लोकसौंदर्य का उन्मेष है, जिसमें भय और वीभत्सता का अनुभवसिक्त नीला रंग भी मिला हुआ है।
इसका मतलब यह भी नहीं कि अग्निशेखर के कवि का बिम्ब हमेशा चेतन-मन से ही नहीं उपजता है, वरन बीच-बीच में उसमें स्मृति और अवचेतनता भी उतनी ही दिखती है, जिसे फैंटेसी या स्वप्न के माध्यम से भी कवि चित्रित करने में सफल हुआ है मेरे दोस्त ने सपने में सुने मुझे कविता
मास्को में हिमपात
इतने में चली आई माँ भी कहीं से मेरे
मेरे चेहरे पर गिरने लगे
मास्को की बर्फ के आवारा फाहे
कुछ अदृश्य छीटे
छुआ मेरी माँ ने आश्चर्य से
मेरे विस्मय को
दग था वहीं खड़ा
मेरे कवि दोस्त भी
गिर रही थी जैसे सदियों बाद बर्फ
जैसे पहली बार भीग रहा था मैं
किसी के प्रेम में
मै आँख मूँदकर निकल पड़ा उस क्षण
बचपन की गलियों
खेत खलिहानों में निर्वासन के पार
बरस दर बरस
और बर्फ गिर रही थी झूम झूमकर
हमारे हाल पर
समय के कमाल पर
यह फैंटेसी उदय प्रकाश की फैंटेसी कविता रात में हारमोनियम की तरह हमें चौकाती नहीं, न कोई अनर्गल प्रलाप ही करती है, बल्कि कविता की अंतर्वस्तु को मुक्तिबोध की अंधेरे में कई तरह समकालीन सच की परतों को उघाड़ती है। कवि के अनुभवों के कई लेयर होते हैं, उसके अनुभूत संसार का जो हिस्सा उस समाज (यहाँ कम्युनिटी कहना बेहतर होगा) से जाकर जुड़ता है, जिसके यथार्थ को उसने भोगा-सहा है, वह अनुभव कविता को उस कम्युनिटी से जोड देता है। फिर वह अनुभव कवि का व्यक्तिक अनुभव नहीं रह जाता। प्रसंगात अग्निशेखर की कविताएँ निर्वासित समाज के उसी अनुभूत यथार्थ का प्रतिबिम्ब है। इस बात को समझने में हमें भूल नहीं करना। चाहिए कि यह कवि का आत्मनिर्वासन नहीं है।
इस प्रसंग में डॉ उषा रानी राव कहती हैं कि इन कविताओं की अंर्तधारा आत्मपीडित यथार्थ में सर्वजनीन • वेदना का व्यापक स्वर है। वास्तव में इन कविताओं को पढ़ते हुए जो पीड़ा होती है, वह कवि की एकल नहीं है। इस पर युवा समालोचक और कवि भरत प्रसाद व्यक्त करते हैं कि अग्निशेखर जी का नाम ऐसे कवियों में शुमार हैं, जो कविताएं लिखते ही नहीं, बल्कि उसे जीते हैं, भोगते है, कधा से कधा, कदम से कदम मिलाकर चलते है। विशेष तौर पर बेवतनी की अकथ पीडा, क्रोध और तडप को उन्होंने जिस तीक्ष्णता और हिम्मत से काव्यबद्ध किया है वह मानीखेज है। स्वर एकादश के प्रवेशद्वार कवि रहे अग्निशेखर इधर उनकी नवीनतम कविताओं में गुणात्मक परिवर्तन लगातार बना हुआ है, जो कि उनके प्रतिरोधी व्यक्तित्व के बदौलत ही जीवित है। इस बावत प्रख्यात चित्रकार और लोकधर्मी कवि रविन्द्र कुँअर कहते हैं कि वह सिर्फ उस कवि की ही पीड़ा नहीं है, उस पूरे घाटी (कश्मीर) की पीड़ा है। कहना होगा कि पीड़ा की यह आकुलता जिस कलात्मकता से उनके कवि को रूपायित करता है, वह उनकी कविता के प्रतिमानों को श्रेष्ठ बनाता है। यह कवि की अर्जित अंतर्दृष्टि से ही सम्भव हो पाता है जिसमें उसका व्यक्तित्व और कविता दोनों एक-दूसरे के बरक्स खड़े होते हैं अर्थात एकमेक हो जाते हैं। इससे कवि की आंतरिक और बाह्य दुनिया को अच्छी तरह समझा जा सकता है। इस दृष्टि से सोचा जाए तो अग्निशेखर के जीवन और कवि में कोई फॉक नजर नहीं आता।
बिहार के लोकप्रिय युवा लोकधर्मी कवि राजकिशोर राजन अग्निशेखर की कविताओं पर टिप्पणी देते हुए। "आगे कहते हैं कि इन दिनों की कविता में यह विरल काव्य गुण शायद ही किसी अन्य कवि में हो। कला और भाव के अनूठे संयोजन से इनकी कविताएँ एक नया आस्वाद पैदा करती हैं। उनके ही शब्दों में यह वर्तमान उस और दिशाहीन आलोचना का समय ही है कि ऐसे महत्वपूर्ण कवि को नजरदाज किया गया है। गोया कि अग्निशेखर जी की कविताएँ अपने शिल्पगत विशेषताओं के साथ अंतर्वस्तु के कारण भी महत्वपूर्ण हैं। राजन आगे कहते हैं कि वे एक योद्धा कवि हैं। विस्थापन की पीडा ही नहीं उसकी लड़ाई भी वे लड रहे हैं, यानी कवि का जीवन भी कवि जैसा ही है। ऐसे कवि से सिर्फ हम नहीं, कविता का परिवेश भी समृद्ध होता है। इसी प्रकार बिहार से युवा कवयित्री डॉ. भावना का मत है कि स्वानुभूत यथार्थ के जमीन से उपजी अग्निशेखर की कविताएँ इसी कारण हृदय को ज्यादा छूती हैं।
प्रसंगवश यहा रेखांकित करना जरूरी लगता है। कि कवि का यह स्वानुभूत यथार्थ इकहरा और उतना सिम्पल नहीं है, जितना हम समझ बैठते हैं। सादे शब्दों की बानगी में इसमें जीवन के जिस दुर्दधर्ष संघर्ष और दुर्घटनाओं का संगुफन और संश्लिष्टता विद्यमान हैं, उसके कई प्रस्तर (लेयर) हैं। मुक्तिबोध की तरह उनकी कविताओं में संवेदना का सश्लिष्ट रूप अंतर्वस्तु और शिल्प के कई पहलों में दृष्टिगोचर होता है। जिस तरह फैंटेसी का सार्थक उपयोग मुक्तिबोध की कविताओं में देखने को मिलता है, उसी प्रकार जलावतनी की पीड़ा और संवेदना विचारों के जिस लयात्मक और कलात्मक प्रवाह और तीव्रता के साथ अग्निशेखर के यहां प्रकट होती हैं, वह कवि के यथार्थ बोध के वस्तुनिष्ठ अध्ययन के कई नए द्वार खोलता है यथाय विशिष्ट काव्यशिल्प, विचारों का आवेग, अलंकार र विधान, आतंक का सौन्दर्य, भाषाशिल्प, लोकचेतना की स्तुनिष्ठता, कविता की प्रामाणिक भावसत्ता, उसका उतापक्ष उसके वैश्विक मूल्य इत्यादि। बहरहाल, इनकी एक कविता देखिए
एक मैं तुम्हें भेजता हूँ
अपनी नदी की स्मृति
सहेजना इसे
वितस्ता है
कभी यह बहती थी
मेरी प्यारी मातृभूमि में
अनादि काल से
मैं तैरता था
एक जीवन्त सभ्यता की तरह
इसकी गाथा में
अब बहती है निर्वासन में
मेरे साथ-साथ
कभी शरणार्थी कैम्पों में
कभी रेल यात्रा में
कभी पैदल
कहीं भी
रात को सोती है मेरी उजड़ी नींदों में
नदी बहती है मेरे सपनों में
शिराओं में मेरी
इसकी पीडाएँ हैं
काव्य सम्वेदनाएँ मेरी
और मेरे जैसों की
मैं तुम्हें भेजता हूँ स्मृतियाँ
एक जलावतन नदी की
(एक नदी का निर्वासन अग्निशेखर )
ऊपर हमने अग्निशेखर की काव्यात्मकता के कई पहलुओं पर गौर किया है। लिहाजा, किसी रचना में अंतर्भूत कला का विश्लेषण जब उसकी अतर्वस्तु और • सोद्देश्यता के आधार पर की जाती है तो उससे रचनाकार की पक्षधरता का पता चलता है। यह पक्षधरता साहित्य में प्रतिबद्धता बनकर तब सामने आती है, जब कवि का नैतिक बल मजबूत हो। प्रतिबद्धता मात्र कला या शिल्प-सौंदर्य के विकास से अर्जित नहीं की जा सकती, न ही वह कवि के काव्य-ज्ञान अर्जित परम्पराओं या उसके समाजशास्त्रीय अनुभवों से फलित होता है, बल्कि वह लोक से अर्जित नैतिकता और सुसस्कार फलित होता है। अग्निशेखर ने अपनी कविताओं में जिस सामाजिक चेतना का निरंतर विकास किया है, उसकी भावभूमि उस उजड़े हुए लोक में वापस लौटने की प्रतिबद्धता से बनता है जहां से वे जलावतन हुए।
इतिहास बताता है कि दुनियाभर में राजनीतिक महत्वाकाक्षा वर्चस्ववाद और घेरेबंदी के परिणामस्वरूप जलावतनी और विस्थापन की घटना सार्वभौम रही है। सभी देशों के इतिहासज्ञों ने इसे बड़ी मानवीय त्रासदी के रूप में रेखाकित किया क्योंकि इससे दुनियाभर में लाखों बेकसूर जिंदगियाँ तबाह हुई बिन वजह हजारों मौत के घाट उतार दिए गए, बल्कि सामुहिक नर-सहार (जीनोसाइड) ने वहां की संस्कृति विशेष के कला साहित्य का भी निर्ममतापूर्वक दमनकर उसके कल्चरल जीनोसाइड को अंजाम दिया। विस्थापन की इन दुखभरी विद्रूपताओं पर पूरी दुनिया में क्लासिक और मार्मिक साहित्य रचे गए, उसको कलात्मक अभिव्यक्तियाँ मिलीं। इस क्रम में देखने वाली बात यह है कि इसका भारतीय काव्यचित्त जितनी उदात्तता, कलात्मकता और प्रज्ञा के साथ कवि अग्निशेखर के काव्य में मिलता है, वह समकालीन अन्य हिंदी कवियों में विरला है। (कश्मीर) घाटी के जलावतनी की अस्मिता और वस्तुसत्य की जो तस्वीर इनकी कविताओं में मिलता है, वह उनके कद को एक चौड़ा पाट प्रदान करता हुआ और एक वैश्विक फलक तक ले जाता हुआ प्रतीत होता है। गोकि जमीन और चीजों के छूट जाने की जो स्मृतिशेष हैं, उससे कवि के अंदर जो नॉस्टेल्जिया उत्पन्न होता है, उस विषाद मात्र से ही उत्कृष्ट कविताओं का सृजन नहीं किया जा सकता। आप विस्थापन से प्रत्युत्पन्न बहुत सारे भारतीय कवियों की कविताएँ देख सकते हैं। लेकिन अग्निशेखर जब अपना घर वापस लौटना चाहते हैं और लौट नहीं पाते हैं तो उनकी स्मृति में वर्षों से संजोये हुए सारे सपने भीत के किले की तरह ढह जाते हैं। उस जगह जाकर भी वे उन भौगौलिकताओं वतन और इति तत्वों को ढूंढ नहीं पाते अर्थात सांस्कृतिक सहार (कल्चरल जीनोसाइड) की उत्पन्न स्थिति और अक्सों के साये में उनके विस्थापन का सदमा दुगुना हो जाता है। सपने के दुबारा टूटने से उनके नॉस्टेल्जिया में कारुणिकता का जो इजाफा होता है, उसकी केंद्रीय संवेदना हमें कहीं न कहीं विस्थापन के बड़े वैश्विक साहित्यकारों के रचना-लक्षण से तुलना करने को मजबूर करता है ।। जैसे कि अग्निशेखर की कविताओं की संवेदना तुर्की के एक बड़े साहित्यकार ओरहान पामुक और इजरायल के आधुनिक कवि यहूदा अमिखाई की केंद्रीय संवेदना से जुड़ती हुई दिखती है। पामुक ने विस्थापन के भीतर विस्थापन (अर्थात वैश्विक साम्राज्यवादी नीतियों व लडाइयों के उपरांत पीड़ित विस्थापितों की पूर्व स्मृतियों का विस्थापन) और दुनिया के दो हिस्सों के बीच मानसिक-वैचारिक टकराहट के बीच जिस संवेदनात्मक तनावों को अपनी कृति में रखा उसके अक्स आपको अग्निशेखर की कविताओं में भी मिलेंगी। मसलन, उनकी एक कविता एक जानलेवा पुस्तक लोकार्पण (जलता हुआ पुल संग्रह) में कवि व्यक्त करता है कि अपनी ही पुस्तक के लोकार्पण के लिए अपनी नदी के एक पुल पर वह सुरक्षा बलों से तनी संगीनों के साये में खड़ा हुआ है, जहां से उसे सब कुछ बदला हुआ नजर आता है। उसका स्कूल वीरान पड़ा है। घर बदहाल सूने से हैं और सुरक्षा बलों ने जल्दी (लोकार्पण) करने का हुक्म दिया। और कवि कहता है
हा, शायद
मैं गंवाने जा रहा था जीवन
पहचान लिया जा सकता था
नदी तटों पर खड़े
सूने बदहाल घरों की किसी भी
अंधेरी खिड़की से आ सकती थी गोली
और पुल से
कविता संग्रह के साथ
मेरी लाश भी नदी में गिर जाती
कितना अच्छा होता
मैं घुल जाता नमक की तरह
नदी के मौन में
मैंने पुल से विसर्जित की
कविताएं वितस्ता में
और देर तक देखता रहा
नदी का रोमाच.
यह विस्थापन के भीतर एक दूसरे विस्थापन के दर्द की ओर इशारा करता है, जहाँ अपने वतन में टिकने के हालात नहीं है, कवि अपने किताब के लोकार्पण को अपनी जमीन पर गया हुआ है, पर ज्यादा देर वहा पुल पर उसे रुकने की इजाजत नहीं है। माहौल इतना खराब है कि सुरक्षा बल जल्दबाजी करने का आदेश दे रहे। इस तरह मानव की स्वतंत्रता वहा पूरी तरह स्मृतिशेष ही हैं। वादियाँ वहाँ पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है, वहां सब कुछ बदल चुका है। चारों और डर और आतंक का साया है। इस संदर्भ को और स्पष्ट करने के लिए जलता हुआ पुल संग्रह की ही एक कविता यह हमारा जीवन के कुछ अंश देखिए
अरे आदरणीय
कसो कसो फब्तियां
हमारे विलोपन पर
मातृभाषा से हमारे बच्चों के कटने पर
हंसो कि जिन्होंने मजबूरी में बेच डाले
खेत, पेड़ और अस्थियाँ पुरखों की
उनके फटे तंबूघर बदले हैं।
वृद्ध आश्रमों में
अरे हंसो
टूटी खिड़कियों से उगी घास
या वीरान अधजले घरों
खंडित देवालयों पर
या बदले जा चुके
हमारे काव्यबिम्बों, प्रतीकों, उपमाओं
रोजमर्रा के मुहावरों पर
हंसो कि यह थी हमारी नियति
अरे हंसो अभी मौका है
उतना ही
जितनी बची है
अजगर के मुह से बाहर
यह पूँछ
रुक रुककर हिलती..
इन कविताओं में विस्थापन की संवेदना केवल एक 'नॉस्टेलजिया भर नहीं है। विस्थापन की मार इतनी गहरी है कि केवल लोग गरीब-अशक्त ही नहीं। हुए धार्मिक आस्थाओं के केंद्र यानी प्रार्थनाओं की जगह और पूजाघर भी खंडित हो गए। उसी प्रकार, हमारे काव्यबिम्बों, प्रतीकों, उपमाओं और रोजमर्रा के मुहावरों बदल जाने का अर्थ कितना गहन-गंभीर है। यहाँ साहित्य भी दासता और मोहताज के शिकस्त हो गए। अजगर के मुह मे रुक रुककर हिलती हुई। निगले जाने वाले निवाले के अंतिम अंश सरीखे बिम्ब को देखिए ! वीभत्सता को रेखांकित करने के इतने सुघड बिम्ब एक ही वाक्यांश में सांस्कृतिक सहार को सलीके से व्यक्त कर रहा है। अग्निशेखर की कविताओं के जलावतन पीडितों के होमलैंड की हालातों को जब यूरोप एवं बाहरी देशों की साम्राज्यवादी ताकतों द्वारा ध वस्तीकरण के पश्चात शरणार्थियों के हालातों से तुलना करेंगे तो आपको लगेगा कि ये आपस में काफी मिलते-जुलते हैं। इस तरह अग्निशेखर की कविताओं में विस्थापित पीड़ितों एवं नागरिकों की अवस्थितियाँ जिस प्रकार चित्रित-व्यजित होती हैं, वह उनकी कविता- प्रतिमानों को दुनियाभर के विस्थापित मशहूर कवियों के कविता प्रतिमानों एवं काव्यात्मक संवेदनाओं के काफी करीब ले आती हैं। अग्निशेखर के कवि का यह गुण शिल्पसौंदर्य और भावसौंदर्य दोनों ही दृष्टियों से अनूठी महत्वपूर्ण और रेखांकित करने के योग्य है। उदारहण स्वरूप उनकी एक कविता और देखिए -
विरसे में गांव
पिता ने गर्व से दिखाई थीं मुझे गांव ले जाकर अपनी जड़ें, खेत खलिहान, नदी, अखरोट और चिनार के पेड़, जो छीन चुके थे पिता से विभाजन के बाद पाकिस्तानी हमले में लेकिन बचा लाए थे वह समूचा गांव अपने हृदय में हम शहर दर शहर बसते- उजडते जहा भी रहे स्मृतियों में रहे अपने गांव में
पिता ने दी यह विरसात एक दिन मुझे सौगंध के
साथ
कि कभी ना भूलू में अपनी जड़े
जनपद अपना नहीं तो वह स्वीकार नहीं करेंगे
तर्पण मेरा
क्या यह पिता को था एक और जलावतनी का
पूर्वाभास
क्या वह देख रहे थे खोदी जा रही हमारी जड़ें,
मालूम था उन्हें स्मृति और एक सोंधी महक
मातृभूमि की रखेगी हमें जिंदा खानाबदोश बरसों
में
मैं लड़ता रहूंगा पिता स्मृतिलोप के खिलाफ और पहुँचूँगा एक दिन हजार हजार संघर्षो के बाद अपने गांव की नदी पर बुलाऊंगा तुम्हें पितृलोक से चिनारों के नीचे पिलाऊगा अजुरी भर-भर तुम्हें वितस्ता का जल,पिता में सांस सास जी रहा हू अपना गांव तुम स्वीकार करो मेरा तर्पण।
(काव्य संग्रह जवाहर टनल से)
यह अकेली कविता कल्चरल जीनोसाइड में निगल लिए गए अपनी सांस्कृतिक धरोहरों को वापस लौटाने के लिए लिखी गई वह स्वप्न-काव्य है, जिसके मिथक और फैंटेसी हमें भीतर तक आलोड़ते ही नहीं, उस लोकचेतना से उस मिट्टी से जोड़ते हैं जो भारतीय होने की थाती है और जिसकी जद्दोजहद और प्रतिबद्धताए कवि को एक वैश्विक आयाम देने से नहीं चूकती।
अस्वीकरण :
उपरोक्त लेख में व्यक्त विचार लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं और kashmiribhatta.in उपरोक्त लेख में व्यक्त विचारों के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं है। लेख इसके संबंधित स्वामी या स्वामियों का है और यह साइट इस पर किसी अधिकार का दावा नहीं करती है। कॉपीराइट अधिनियम 1976 की धारा 107 के तहत कॉपीराइट अस्वीकरण, आलोचना, टिप्पणी, समाचार रिपोर्टिंग, शिक्षण, छात्रवृत्ति, शिक्षा और अनुसंधान जैसे उद्देश्यों के लिए "उचित उपयोग" के लिए भत्ता दिया जाता है। उचित उपयोग कॉपीराइट क़ानून द्वारा अनुमत उपयोग है जो अन्यथा उल्लंघनकारी हो सकता है।"
साभार:- अग्निशेखर, सुशील कुमार एवं जून 2021 कॉशुर समाचार