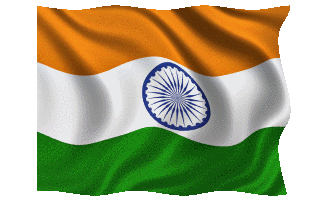कथा डायरी- गालिब, मंटो और कश्मीर

कथा डायरी- गालिब, मंटो और कश्मीर
महराज कृष्ण संतोषी
गालिब और मटो दोनों जन्नत से कश्मीर की सैर को आए ।
मटो ने गालिब से कहा, "मेरे पुरखे यहीं के थे।"
"रहने दो मंटो हमारी वंश परम्परा तो जामे जमशीद सुरा उपासक से शुरू होती है।" गालिब बोला
"बस कुछ और मत कहना. " मंटो ने सुझाया।
"लेकिन क्यों?" गालिब ने उत्सुकता से पूछा।
"क्योंकि यहां शराब और हिन्दुस्तान की बात करना दोनों हराम है।"
मटो शहर में अकेला घूम रहा था कि सिपाही
ने उसे रोका और बोला- "अपना पहचान पत्र दिखाओ?"
"मैं अफसाना निगार हूं।" मटो ने गर्व के साथ
कहा। सिपाही पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
"कहा रहते हो?" सिपाही ने पूछा।
मंटो कुछ सोच में पड़ गया। ऐन इसी वक्त टोबा टेक सिंह दौड़ता हुआ आया और सिपाही से मिन्नतें करने लगा।
"इसे जाने दे जनाब! ये अपने ही अफसाने पढ़ पढ़ कर पगला गया है.
सिपाही समझदार था। उसने मटो को जाने दिया।
गालिब और मंटो डल झील के किनारे टहल रहे थे। गालिब का लिबास मुगलिया दौर का था और मंटो का पहनावा अविभाजित हिन्दुस्तान का। आसपास और लोग भी थे जो उन्हें देख नहीं पा रहे थे। टहलते-टहलते वे पासपोर्ट दफ्तर के नजदीक पहुंचे। वहां काफी लोग जमा थे। पता चला वे सारे लोग पासपोर्ट बनवाने के लिए आए हैं। "इतने सारे लोग कहा जाना चाहते है?" गालिब जानना चाहता था।
"हज के लिए" मंटो ने जवाब दिया। "चलो वापस लौट चलते है" गालिब ने मंटो की बांह पकड़कर कहा।
संध्या का समय। वे दोनों फिर टहलने निकले। थोड़ी दूर चलकर उन्हें खुले मैदान में बहुत सारे लोग दिखे जो पिंजरानुमा दुकान के सामने कतार में खड़े थे।
उन्हें देखकर दोनों एक-दूसरे की ओर देखने लगे । "लगता है खुदा ने हमारी सुन ली" गालिब के स्वर मस्सरत थी। "हा मुसलमान होने का यही तो एक फायदा है
किं खुदा जल्दी सुन लेता है," मंटो के कहने में शरारत दिख रही थी
"हां मंटो, तुम सही फरमा रहे हो। औरों की बाद में सुनता है लेकिन हम जैसे शराबियों को कभी निराश नहीं करता' गालिब ने मुस्कुराते हुए कहा।
गालिब और मंटो को कश्मीर आए हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे। पर वे धरती के इस स्वर्ग की हकीकत जान चुके थे। हर ओर खाकी वर्दी पहने सिपाही ही सिपाही नजर आते थे-अंगुली ट्रिगर पर रखे हुए। कब, कहां, क्या हो कुछ कहा नहीं। जा सकता।
एक दिन वे शंकराचार्य पर्वत की ओर निकल गए। रास्ते में शायद ही कोई आ-जा रहा था। चोटी पर पहुच कर वे पुराने मंदिर के सामने खड़े हुए। उन्हें यह देखकर ताज्जुब हो रहा था कि मंदिर पर भी पुलिस का सख्त पहरा है।
एक सिपाही ने उन दोनों से कहा कि दर्शन करने से पहले वे रजिस्टर में अपना नाम पता लिखें। दोनों ने ऐसा ही किया। सिपाही ने उनके लिखे को देखा पर उसे उर्दू पढना नहीं आता था। वह रजिस्टर को उर्दू-जानकार सिपाही के पास ले गया। वह बोला कि "इन्होंने अपना नाम गालिब और मटो लिखा है।"
"क्या आप दोनों हिन्दू नहीं है?" सिपाही ने हैरानी के साथ पूछा।
"ख़ुदा से पूछकर बताएंगे गालिब ने जवाब दिया।
यह सुनकर मंटो हंसा और सिपाही को भी हंसी आ गई।
मंटो और गालिब वापस लौटने की तैयारी कर रहे थे। धरती का स्वर्ग उन्हें रास नहीं आ रहा था। 1 लौटने से पहले वे अतिम बार सैर करने को निकले। चलते-चलते वे परीमहल पहुचे। वहां के आसपास को देखकर उनके मुंह से एक साथ निकला. "वाह!"
गालिब बोला, "लगता है यहां किसी नेक और आलिम आदमी की रूह बसी हुई है।"
मंटो को याद आया उसने इतिहास में पढ़ा था कि दाराशिकोह का कुतुबखाना श्रीनगर के परीमहल में स्थित था। यहां वह ज्ञान की साधना करता था। मंटो सचेत हुआ। यह वही परीमहल था-बाहर बोर्ड पर भी लिखा है वह सोचने लगा कि जो नहीं होना चाहिए था वही होकर रह गया।
दाराशिकोह बदनसीब निकला। औरंगजेब राजपाठ छीनकर हिन्दुस्तान का बादशाह बन गया।
मंटो को दुख हुआ कि उसने अपने जीवन में दाराशिकोह पर कोई कहानी क्यों नहीं लिखी। वह फिर सोच में पड़ गया। अगर दाराशिकोह हिन्दुस्तान का बादशाह बन गया होता तो क्या इस मुल्क का इतिहास कुछ अलग नहीं होता।
इधर गालिब जैसे परीमहल की खूबसूरती में खो गया लगता था। उसे जगाते हुए से मंटो ने कहा "आओ गालिब हम दोनों यहां सजदा करते हैं।"
"क्या कहा सजदा करते हैं।" गालिब ने हैरत के साथ कहा।
"हा सजदा करते हैं।"
"क्या यहां कोई सूफी रहा है।"
"हां गालिब ! एक ऐसा सूफी जो बादशाह तो नहीं बन सका लेकिन अनगिनत लोगों के दिलों का शहंशाह जरूर बन गया।"
"तब हम भी उसे जानते होंगे" गालिब ने कहा।
"हां-हां अच्छी तरह से।"
"क्या नाम था इस शहंशाह का।" "दाराशिकोह " नाम सुनते ही गालिब की आखों में आंसू आ गए।
कहते है इसके बाद वे दोनों कहीं नहीं दिखे। जहां से आए थे शायद वहीं लौट गए होंगे।
हम भूल गए है
अपने मुसलमान पड़ोसियों को
पर वे इतने बुरे नहीं
हम उजड़े लोगों का दर्द समझते हैं
तभी हमारे घर खरीदकर
हमारी आर्थिक सहायता करते हैं
मा तब जिन्दा थी जब कश्मीर से गुलजू हमारे यहां आए थे। तब हम किराए के मकान में रहते थे। दो कमरों वाले इस घर में हम घुट-घुटकर जीने के अभ्यस्त हो चले थे।
गुलजू ने हमारी हालत देखी तो उसे आंसू आए। बीते दिनों को लेकर चर्चा की। मेरे पिता की यारभाषी को भी याद किया। गुलजू कश्मीर में हमारा पड़ोसी था। गरीबी में दिन गुजर रहे थे। पर अब सुना है कि आलीशान घर में रह रहे हैं। सभी बच्चे सरकारी नौकरी कर रहे है।
मैंने उसे गौर से देखा उसकी घनी दाढी थी। लिबास भी हमसे कुछ अलग था। मां उसे पहले पहचान ही नहीं पाई। पर जब यह पता चला कि वह गुलजू है तो हंसने लगी। मा को ऐसे पहले कभी हसते नहीं देखा था
"गुलजू आप तो पहले दाढ़ी नहीं रखते थे। मा बोली।
"माहरा यह हमारा मजहबी फरमान है। मुसलमान होने का सबूत।" गुलजू बोला।
""तो क्या पहले मुसलमान नहीं थे?" मा की आंखों में तनिक शरारत थी। मैंने मां की तरफ इस तरह देखा कि वह समझ गई। चुप्पी में समय बीता जा रहा था। फिर जिस कारण से गुलजू हमारे यहां आए थे, उसे उन्होंने जाहिर कर ही दिया। बोला "आपका मकान रहने लायक नहीं रह गया है। अच्छा होगा कि आप इसे बेच ही डालें। मैं खरीदने को तैयार हूं। सब रूपया एकमुश्त दूंगा। उस पैसे से यहां नया मकान बनाना। आखिर कब तक किराए के मकान में रहोगे। मुझसे सचमुच आप की हालत देखी नहीं जाती।"
"यह रहा मेरा फोन नम्बर " गुलजू उम्मीद की नजरों से हमारी ओर देख रहा था।
मैंने खुद ही खुद को चिट्ठी लिखी
मैंने खुद ही खुद को जवाब दिया
अब वह इस पते पर नहीं रहता
मन बावरा है। जो नहीं है उसे ही चाहता है। जो भूलना सुखकर है वही याद दिलाता रहता। थोड़ा-सा भी एकांत मिले तो पुराने दिनों में लौट जाता है। वे दिन अच्छे भी थे और बुरे भी पर सब एक साथ रहते थे। अब एक-दूसरे को देखे महीनों बीत जाते हैं। फोन तो बस औपचारिकता है। कभी सोचा नहीं था कि इस तरह अपनी मातृभूमि से पलायन करना पड़ेगा। इतने बरस बीत गए लेकिन मिट्टी का बना अपना वह घर आखों में ही बसा हुआ है।
खिड़की खोली नहीं कि चारों ओर हरापन दिखाई देता है-आत्मा को तरोताजा रखने वाला हरापन। चारों ओर सादगी का आलम था। एक जैसे थे हम सब मानो हमशक्ल हों। कभी-कभी एक-दूसरे से लड़ते जरूर थे पर फिर मेल-मिलाप में बंध जाते। एक जैसी कहानियां थीं हमारी सुख-दुख के लिए एक जैसे गीत थे। तब किसी ने नहीं कहा कि हीमाल-नागराय किस धर्म से हैं। अकनदुन गाथा गीत सुनकर हर किसी की आंख नम होती। कहां गए वे दिन !
इतिहास खंगालता हूं तो भय लगने लगता है। सूफी चोला पहने अपने ही लोगों की भाषा मिथ्या है। नई तहजीब का असर हर कहीं साफ दिखता है। ऐसे लगता है जैसे कालीन ने घास की चटाई को निगल लिया है। सोचता हूं जहां से हमें निकाला गया वहां का पता पीढ़ी-दर-पीढ़ी याद रखना बेहद जरूरी है। क्या पता कब हमें अपना होना प्रमाणित करना पड़े।
तुम पीठ पर
किसका बोझ ढो रहे हों
अपने इतिहास का
इसे उतार क्यों नहीं देते?
इसे रखने के लिए
हमारे बच्चों के पास जगह नहीं है
हम अधिकतर अपने अतीत के ही बारे में सोचते रहते है। क्या यह हमारी उम्र का तकाजा है या हमारी लाचारी अतीत का मोह पाले बिना हमारे पास कोई दूसरा विकल्प भी तो नहीं। हममें से अधिकतर अपना आधे से अधिक जीवन कश्मीर में ही बिताए है जो हमारे मनोविज्ञान का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। हमारे बच्चों के पास खुद को साबित करने की चुनौती है। वे भविष्य की सतानें हैं। उनके पास लम्बी-लम्बी उड़ानों के हौसले हैं। क्या हमें उनके सपनों में जीना नहीं चाहिए?
कितना भी हम विवेक सम्मत हो जाए पर हम इतिहास की जकड़ से मुक्त नहीं हो सकते। हम इतिहासजदा हैं। जातीय सहार के किस्से हमारे विरसें में आए है। कहा छोड़ आए इन्हें इतिहास पढना जरूरी है और याद रखना मजबूरी यह हमें हमारी पहचान देती है। क्या हमारी यह पहचान हमारे बच्चों की नियति से जुड़ी हुई नहीं है? वे मनीप्लांट के पौध तो हैं नहीं वे तो चिनार के वंशज हैं।
दरवाजा खुल रहा है
नहीं, दरवाजा खोला जा रहा है
पुलिस हो तो जयहिन्द कहना
मुजाहिद हो तो पाकिस्तान जिन्दाबाद
कहते है जब लोगों पर ज्यादतिया होने लगती है तो वे अंतरात्मा का सच छिपाने लगते हैं और एक छद्म भाषा का प्रयोग करने लगते हैं। जान की सलामती के लिए यह अनुचित भी नहीं कहा जा सकता।
समय की उथल-पुथल में हम यह भाषा बोलने के आदी हो गए हैं। आज हम अपने इस भाषाई गुण से शत्रु और मित्र दोनों को भ्रमित करते हैं।
हम जहां कहीं भी बस जाते हैं
कसाई अपने आप वहां आ जाते हैं
हम और क्या सबूत दें
अपने अहिंसक होने का
हम कश्मीरी पंडित आचार, विचार और व्यवहार में अहिंसक होते हैं लेकिन हम ऐसे कट्टर मांसाहारी ब्राह्मण हैं जो शिवरात्रि पर भगवान शिव को मांस का भोग चढ़ाते हैं और गर्व करते हैं अपनी इस निरामिष परम्परा पर। हमारे यहां के कसाई पुज कहलाते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि पुज शब्द की व्युत्पत्ति पुजारी शब्द से है। यह कहा तक सही है, इसे भाषा वैज्ञानिक ही बता सकते हैं। पर हम अपनी मास प्रियता के लिए बखूबी जाने जाते है। कश्मीर से विस्थापित होने के बाद भी हम अपने कसाई भाई को भूले नहीं हैं और वह भी हमें भूला नहीं है। यहीं हमारे पास चला आया। हम भले ही कश्मीरी मुसलमान से त्रस्त रहे हों पर कसाई से हमारा लगाव अटूट है। हमारी शांतिप्रियता मांस खाने से ही पोषित होती आई है। यह अकारण नहीं है कि शताब्दियों तक बौद्ध धर्म का यहां वर्चस्व बना रहा। हम थक जाते हैं तो मांस खाते हैं। हम उदास हो जाते हैं तो मास खाते हैं। हम कोई व्रत रखते हैं तो अगले दिन सबसे पहले कसाई की दुकान पर जाते हैं। मुझे लगता है कसाई हमारे दिल में है या यह कहें कि हम ही कसाई के दिल में हैं।
हम सबसे पहले
अखबार में निधन समाचार पढते हैं
और अपने सकुशल होने का
भ्रम पालने लगते हैं
मृतक अखबार नहीं पढते
फिलहाल यही एक सबूत है
हमारे जिन्दा होने का
कश्मीर के हमारे गांव में कभी अखबार नहीं आता था। उन दिनों रेडियो से ही समाचार सुनने पर तृप्ति मिलती और लोग चैन की नींद सोते ऐसा भी नहीं कि कश्मीर उन दिनों शांत था। हा, गड़बड़ी के दिनों में लोग बी.बी.सी. सुनकर समाचारों की पुष्टि जरूर करते।
मैंने सबसे पहले जो अखबार हाथ में लिया वह उर्दू अखबार मिलाप था जो जालन्धर से निकलता था। यह 1969 के आसपास की बात है। इस अखबार में फिक्र तोसवी का एक कॉलम प्याज के छिलके नाम से हर रविवार पढ़ने को मिलता। इसे पढ़ना मुझे बहुत भाता था। पर दिक्कत यह थी कि यह हमारे पास डाक से आता था और डाकिया की मर्जी से हमें यदा-कदा ही मिल जाता था। गांव का कोई भी बाशिंदा इसे डाकिया से लेने का हकदार बन गया था। एक स्थानीय अखबार आफताब भी गांव में कोई कोई पढ़ता था। इसमें खजर सोचता है वलुर के किनारे से एक कालम पढ़ने को मिलता। साथ में एक स्थाई चित्र भी रहता जिसमें किसान की टोपी में एक आम आदमी हुक्का पीते हुए दिखता था।
उन दिनों यह माना जाता था कि मनन-चिन्तन हुक्का काम आता है। कोई भी समाधान तलाशना में हो तो कुछ क्षण हुक्का गुडगुडाए और हल मिल गया। मेरे पिता जी का यह हुक्का फलसफा हमारे परिवार में सर्वमान्य था। आज भी मुझे कश्मीर का खजर हुक्केवाला याद आता है। तीस बरसों से उसे एक बार भी नहीं देखा। पता नहीं कहा होगा और क्या सोच रहा होगा। जिन्दा भी होगा या हालातों की मार से डरते-डरते सोचने का आदी बन गया होगा। वैसे उन दिनों हम अखबार चाव से पढ़ते थे। आज की तरह नहीं कि देखें ज्यादा और पढ़ें कम ।
आज हमारे विस्थापन में अखबार देखना हमारी मजबूरी बन चुका है। अखबार आया नहीं कि हम निधन समाचार देखने लगते हैं। जातीय भावना से हम इन मृतकों को मूक श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं। उदास भी हो जाते हैं। फिर नमकीन चाय की चुस्किया लेते हुए यह उदासी काफूर हो जाती है और हमारा कर्तव्यबोध जाग जाता है। मेरा एक दोस्त कहता है कि "हम कश्मीरी पंडितों की एकता मृतक के दसवें दिन प्रकट होती है या फिर विवाह के महाभोज पर। शेष दिन हम अपनी डफली अपना राग लेकर ही जीने में विश्वास रखते है।"
यह मरघट भूमि है
मगर इस समय
प्यार करने के लिए
सबसे सुरक्षित जगह है
शरणार्थी शिविरों में प्यार-मोहब्बत सब स्थगित है। तम्बुओं की बस्ती में एक-दूसरे की सांसें भी सुनाई देती हैं। यहां प्यार करने की न कोई उम्मीद है न कोई राह ।
उस दिन बस्ती से तनिक दूर मरघट भूमि के आसपास एक विस्थापित युवा जोड़ा अश्लील हरकतें करता हुआ देखा गया। जहां हम सबको दुखी होना चाहिए था वहीं हम एक-दूसरे के हाल पर हंसते हुए दिख रहे थे।
तुम्हारे पास शहीदों का कब्रिस्तान है
हमारे पास जिन्दा लाशों के लिए
सरकारी आवास है
रोज खबरें आती हैं कि एक और शहीद हुआ। कश्मीर के इतिहासपुरुष खुश हैं कि शहीदों का कब्रिस्तान फैल रहा है और एक दिन जरूर रंग लाएगा। इस रंग शब्द से ही मुझे डर लगने लगता है। जब रंग परस्पर लड़ने लगते हैं तो तमस फैलता है और जब रंग एक-दूसरे में घुले हुए होते है तो रोशनी बन जाते हैं।
उसने जेल में बांटे ताबीज
उसके ताबीज बांधे पुलिस वालों ने
हत्यारा अगर खुदा दोस्त हो
तो पुलिस भी डरती है
उनका भेजा आतंकवादी हमारी जेल में बंद था। कहते हैं वह अपने मजहब का कट्टर पाबंध था। हर वक्त तस्बीह के साथ दिखता। जेल में भी पाच नमाजे पढ़ता। हमारा समाज ऐसे लोगों को खुदा दोस्त कहता है। कहते हैं यह आतंकवादी जेल में खामोश रहा करता था। वह हमारे शहर की जेल में लाया गया था। उसकी खामोशी और खुदापरस्ती को खाकी वर्दी वाले इज्जत देने लगे थे। कई पुलिस वालों को उसने ताबीज भी दे दिए थे। मैंने स्थानीय पत्र में यह सब पढ़ा है। ताबीज लेने वालों में एक ही धर्म के लोग नहीं थे। फिर सरकारी हुक्म से उसे जेल से निकालकर कांधार ले जाया गया विमान अपहर्ताओं ने जेल से उसकी रिहाई की शर्त जो रखी थी।
आज भी जब कभी टेलीविजन पर उसकी तस्वीर देखता हू तो दिमाग में जैसे धुआ फैलने लगता.....
यह क्या बज रहा है?
हमारे न होने की धुन !
इसे कौन सुन रहा है?
वही जो इसे बजा रहा है!
सुनना भी एक कला है। पर हम यह कला सीख नहीं पाए हैं। हम एक-दूसरे को कभी सुनना पसंद नहीं करते। बस अपनी ही सुनाना चाहते हैं। माना सुन भी लिया पर हमें सुनाने वाले पर कतई विश्वास नहीं होता। इसी अविश्वास के कारण हम एकता के सूत्र में बंध नहीं पाते। विस्थापन के शुरुआती दिनों में यह जरूर लगा था कि हम एक-दूसरे को सुनना सीख गए हैं। पर यह सपना बहुत जल्दी टूटा । संगठित संघर्ष की हवा फुस्स हो गई। अपनी मातृभूमि जाने के इच्छुक लोगों के अनेक महंत बन गए और एक महंत दूसरे महंत से कमतर थोडे ही हैं। परिणाम निश्चित था फूटी आंख विवेक की जो हमारे विस्थापन से भी अधिक त्रासद हैं।
जेल में
हत्यारे ने पढी
गांधी की आत्मकथा
जेल से छूटते ही उसने गांधी जी को अपना राजनीतिक आदर्श माना। एक पूरी जाति की बरबादी का नायक अब शांतिप्रियता की बातें करने लगा है। आज वह कद्धावर नेता बनने की कवायद करने लगा है। वह शहर के जिस इलाके में रहता है, वहां कभी वेश्यावृत्ति होती थी।
पता नहीं वह कश्मीर के इतिहास का कितना जानकार है लेकिन इतना तो वह जानता ही होगा कि गांधी के पास सच की ताकत थी । अंतरात्मा की शुद्धता थी। उसके पास क्या है? वैसे ये सभी कश्मीरी नेताओं से पूछा जाना चाहिए। इन नेताओं के तेवर जो भी हों ये असल में लोगों की अस्मत के सौदागर हैं। वे सौदा करते हैं लोगों के सपनों का, उनकी उम्मीदों का, उनके भोलेपन का उनकी वफादारी का......
तुम्हारे पुरखे कौन थे?
पंडित
तुम्हारे उस्ताद कौन थे?
पंडित
तुम्हारे दोस्त कौन थे?
पंडित
तुम्हारे दुश्मन कौन हैं?
पंडित
हम कश्मीरियों के परस्पर रिश्ते एक सिक्के की तरह हैं। एक तरफ दोस्ती दिखती है एक तरफ दुश्मनी। हमारे रिश्तों का यह विरोधाभास बाहरी लोगों की समझ से परे है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हम एक-दूसरे के सुख-दुख में शरीक रहे हैं पर दिक्कत तब होती है जब कश्मीरी मुसलमान दारुल इस्लाम पर अपनी सोच केन्द्रित करने लगता है। तब हम उनके लिए काफिर बन जाते हैं और काफिरों का क्या हश्र होना चाहिए, यह किसी से छिपा नहीं है।
सोचता है कि आखिर हम क्या हैं? काफिर या हू अल्पसंख्यक? या फिर दोनों? हमारा होना क्या उन्हें अपनी क्रूरता की याद दिलाता है? शायद नहीं। वे तो बस अपने धर्म का पालन कर रहे होते हैं। इतिहास तो यही कहता है।
वे कहते हैं
आओ
हम कहते हैं
बुलाओ फिलहाल यही है
हमारा भाईचारा
विस्थापन के इन तीस बरसों में, याद नहीं, किसी मुस्लिम मित्र ने हमारा हाल जानने की कोशिश की हो। जब कभी इन दोस्तों से बात होती है तो वे अपना ही दुखड़ा सुनाने लगते हैं। कहते हैं हम सरकारी बंदूक और जेहादी बंदूक के बीच सांस लेते हैं। संतुलन बिगड़ा तो खैर नहीं। हमारी व्यथा को अनसुना करने के लिए क्या यह उनकी चालाकी तो नहीं है? हमसे हमारी मातृभूमि छिन गई। हम अनिकेत हुए। हम नई आबोहवा का कहर सहन कर रहे हैं। हमारे बुजुर्गों ने मरते समय। अपने ईश्वर का नाम नहीं लिया। वे बुदबुदाते रहे। कश्मीर! कश्मीर!
इधर सियासी लोग दोहराते नहीं थकते कश्मीरियत! कश्मीरियत। तब हमारा दर्द खौलने लगता है। हमारे लिए तो कश्मीरियत बस फटा हुआ दूध है... जो हमारे किसी काम का नहीं रहा....
बहुत पुराने हो गए थे हमारे मंदिर
बहुत बूढ़े हो गए थे हमारे ईश्वर
नहीं भाग सकते थे हमारे साथ
हमने विस्थापन में अपनी आस्था खंडित नहीं होने दी। हमने अपने देवी-देवताओं की अनुकृतियां बनाकर उन्हें प्रतिष्ठित किया। अपनी पूजा-अर्चना में हम बिल्कुल मौलिक हैं। यह और बात है कि हमारे ईश्वर डुप्लीकेट हैं। कभी यह सोचते हुए दुख भी होता है और हंसी भी आती है कि जिन देवी-देवताओं से हम अपने सुरक्षित जीवन की कामना करते हैं, वही हमारी मातृभूमि में पुलिस के पहरे में अपने वजूद को बचाए हुए हैं। उनकी असुरक्षा में हम अपनी भी असुरक्षा देखते हैं। उनके अकेलेपन में हमें अपना भी अकेलापन दिखाई देता है।
खुदा हाफिज मत कहो
अल्लाह हाफिज में भाईचारा है
जब हम भाईचारे की चाह मजहब के आधार पर करें तो वह मानवता के लिए अमंगलसूचक है। क्या पता यह भाईचारा भविष्य में क्या रूप ले ।
सोचता हूं क्या यह मुझ जैसे एक अल्पसंख्यक की मानसिकता है यह उसका स्वाभाविक डर? दुनिया में हर कहीं अल्पसंख्यक क्या ऐसे ही सोचता है? जो मानवता से पहले धर्म, जात, रंग या नस्ल को श्रेष्ठतर मानता है, वही तो है मानवता का असली दुश्मन। उन्हीं से तो डर लगता है.....
हम सूर्यवंशी नहीं
सूर्यमुखी हैं
फूल चुनने के पीछे भी आदमी का मनोविज्ञान काम करता है। पिछली बार जब मैं कश्मीर गया तो देखा कि हर ओर सूर्यमुखी फूल खिले हुए हैं। आगन-आंगन पीले फूल देखना अच्छा लगा पर सोच में भी पड़ गया कि क्या वफादारी सूर्यमुखी फूल जैसी होनी चाहिए? पर जहां वफादारियां चांद की तरह घटती बढ़ती रहती है वहां सूर्यमुखी फूलों का होना व्यवसाय के अतिरिक्त और क्या हो सकता है।
ऐ खुदा !
हमें उन के खुदा से बचा
उस दिन हम सब त्रस्त थे। क्या पता सुबह तक जिन्दा भी रहेंगे। उनके लिए हमारा होना दूसरे खुदा का भी होना है। वे चाहते हैं धरती पर उनके ही खुदा का निजाम चले। वे हमारे खुदा से डरते नहीं पर हम उनके खुदा से जरूर डरते हैं। हम जब इतिहास पढ़ते हैं तो डर जाते हैं। हमारे पुरखों की नियति क्या हमारी भी नियति है? जितना सोचते हैं उतना ही सिहर जाते है। क्या हमें अपना इतिहास भूल जाना चाहिए?
अस्वीकरण :
उपरोक्त लेख में व्यक्त विचार लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं और kashmiribhatta.in उपरोक्त लेख में व्यक्त विचारों के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं है। लेख इसके संबंधित स्वामी या स्वामियों का है और यह साइट इस पर किसी अधिकार का दावा नहीं करती है।कॉपीराइट अधिनियम 1976 की धारा 107 के तहत कॉपीराइट अस्वीकरणए आलोचनाए टिप्पणीए समाचार रिपोर्टिंग, शिक्षण, छात्रवृत्ति, शिक्षा और अनुसंधान जैसे उद्देश्यों के लिए "उचित उपयोग" किया जा सकता है। उचित उपयोग कॉपीराइट क़ानून द्वारा अनुमत उपयोग है जो अन्यथा उल्लंघनकारी हो सकता है।
साभार:- महराज कृष्ण संतोषी एंव दिसम्बर 2022 कॉशुर समाचार